1.संविधान का निर्माण

संविधान निर्माण से पहले के साल काफी उथल – पुथल वाले थे।
यह महान आशाओं का क्षण भी था और भीषण मोहभंग का भी।
15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद तो कर दिया गया किंतु इसके साथ ही इसे विभाजित भी कर दिया गया।
लोगों की स्मृति में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन अभी भी जीवित था जो ब्रिटिश राज के खिलाफ संभवत : सबसे व्यापक जनांदोलन था।
विदेशी सहायता से सशस्त्र संघर्ष के जरिये स्वतंत्रता पाने के लिए सुभाष चंद्र बोस द्व्रारा किए गए प्रयास भी लोगों को बखूबी याद थे।
1946 के वसंत में बम्बई तथा अन्य शहरों में रॉयल इंडियन नेवी
( शाही भारतीय नौसेना ) के सिपाहियों का विद्रोह भी लोगों को बार – बार आंदोलित कर रहा था।
लोगों की सहानुभूति सिपाहियों के साथ थी।
चालीस के दशक के आखिरी सालों में देश के विभिन्न भागों में मजदूरो और किसानो के आंदोलन भी हो रहे थे।
व्यापक हिन्दू- मुस्लिम एकता इन जनांदोलनों का एक अहम पहलू था।
इसके विपरीत कांग्रेस और मुस्लिम लीग, दोनों प्रमुख राजनितिक दल धार्मिक सौहार्द्र और
सामाजिक समरसता स्थापित करने के लिए सुलह-सफाई की कोशिशों में नाकामयाब होते जा रहे थे।
अगस्त 1946 में कलकत्ता में शुरू हुई हिंसा के साथ उत्तरी और पूर्वी भारत में
लगभग साल भर तक चलने वाला दंगे-फसाद और हत्याओं का लंबा सिलसिला शुरू हो गया था
बर्बर हिंसा का यह वीभत्स नाच भीषण जनसंहारों के साथ हुआ।
इसके साथ ही देश-विभाजन की घोषणा हुई और असंख्य लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे।
15 अगस्त 1947
15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस पर आनंद और उम्मीद का जो माहौल था
वह उस समय के लोगों को कभी नहीं भूलेगा।
लेकिन भारत के बहुत सारे मुसलमानों और पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं व सिखों के लिए यह निर्माण चुनाव का क्षण था।
उनके सामने यह तत्क्षण मृत्यु तथा पीढ़ियों पुरानी जड़ों से उखड़ जाने के बीच चुनाव का क्षण था।
करोड़ों शरणार्थी यहाँ से वहाँ जा रहे थे।
मुसलमान पूर्वी व पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ़ तो हिंदू और सिख पश्चिमी बंगाल व पूर्वी पंजाब की तरफ़ बढ़े जा रहे थे।
उनमें से बहुत सारे कभी मंज़िल तक नहीं पहुंचे, बीच रास्ते में ही मर गए।
नवजात राष्ट्र के सामने इतनी ही गंभीर एक और समस्या देशी रियासतों को लेकर थी।
ब्रिटिश राज के दौरान उपमहाद्वीप को लगभग एक-तिहाई भू-भाग छोटे नवाबों
और रजवाड़ों के नियंत्रण में था। जो ब्रिटिश ताज की अधीनता स्वीकार कर चुके थे।
उनके पास अपने राज्यों को जैसे चाहे चलाने का सीमित हक़ ही सही लेकिन काफी आज़ादी थी।
जब अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ा तो इन नवाबों और राजाओं की संवैधानिक स्थिति बहुत अजीब हो गई।
एक समकालीन प्रेक्षक ने कहा था कि कुछ महाराजा तो
“बहुत सारे टुकड़ों में बंटे भारत में स्वतंत्र सत्ता का सपना देख रहे थे।”
संविधान सभा की बैठकों इसी पृष्ठभूमि में सम्पन्न हो रही थीं। बाहर जो कुछ चल रहा था
उससे संविधान सभा में होने वाली बहस और विचार-विमर्श भी भला अछूता कैसे रह सकता था?
1.1 संविधान सभा का गठन

संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था।
1945-46 की सर्दियों में भारत के प्रांतों में चुनाव हुए थे।
इसके पश्चात प्रांतीय संसदों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना। नई संविधान सभा में कांग्रेस प्रभावशाली थी।
प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस ने सामान्य चुनाव क्षेत्रों में भारी जीत प्राप्त की और मुस्लिम लीग को अधिकांश आरक्षित मुस्लिम सीटें मिल गईं।
लेकिन लीग ने संविधान सभा को बहिष्कार उचित समझा और एक अन्य संविधान बना कर उसने पाकिस्तान की मांग को जारी रखा।
शुरूआत में समाजवादी भी संविधान सभा से दूर रहे क्योंकि वे उसे अंग्रेजों की बनाई हुई
संस्था मानते थे और मानते थे कि इस सभा का वाकई स्वायत्त होना असंभव है।
इन सभी करणों से संविधान सभा के 82 प्रतिशत सदस्य कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य थे।
कांग्रेस सदस्य
परंतु सभी कांग्रेस सदस्य एकमत नहीं थे। कई निर्णयों मुद्दों पर उनके मत भिन्न हो सकते थे।
कई कांग्रेसी समाजवाद से प्रेरित थे तो कई अन्य ज़मीदारी के हिमायती थे। कुछ साम्प्रदायिक दलों के करीब थे
लेकिन कई पक्के धर्मनिरपेक्ष | राष्ट्रीय आंदोलन की वजह से कांग्रेसियों को वाद-विवाद करना और मत-भेदों पर बातचीत कर समझौते की खोज करना सीख गए थे।
संविधान सभा में भी कांग्रेस सदस्यों ने कुछ ऐसा ही रुख़ अपनाया।
संविधान सभा में हुई चर्चाएँ जनमत से भी प्रभावित होती थीं।
जब संविधान सभा में बहस होती थी
तो विभिन्न पक्षों की दलीलें अखबारों में भी छपती थीं
और तमाम प्रस्तावों पर सार्वजनिक रूप से बहस चलती थी।
इस तरह प्रेस में होने वाली इस आलोचना और जवाबी आलोचना से किसी मुद्दे पर बनने वाली सहमति या असहमति पर गहरा असर पड़ता था।
सामूहिक सहभागिता बनाने के लिए जनता को सुझाव भी आमंत्रित किए जाते थे।
कई भाषाई अल्पसंख्यक अपनी मातृभाषा को रक्षा की मांग करते थे।
धार्मिक अल्पसंख्यक अपने विशेष हित सुरक्षति करवाना चाहते थे
और दलित जाती – शोषण के अंत की मांग करते हुए सरकारी संस्थाओ में आरक्षण चाहते थे।
सभा में सांस्कृतिक अधिकारों एवं समाजिक न्याय के कई महत्वपुर्ण मुद्दों पर चल रही सार्वजनिक चर्चाओं पर बहस हुई।
1.2 प्रमुख आवाज़ें
संविधान सभा में तीन सौ सदस्य थे। इनमें से छह सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण रही।
इन छह में से तीन — जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेन्द्र प्रसाद — कांग्रेस के सदस्य थे।
एक निर्णायक प्रस्ताव “उद्देश्य प्रस्ताव” को नेहरू ने पेश किया था।
उन्होंने यह प्रस्ताव भी पेश किया था
कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज “केसरिया, सफ़ेद और हरा” रंग की तीन बराबर चौड़ाई वाली पट्टियों का तिरंगा झंडा होगा जिसके बीच में नीले रंग का चक्र होगा।
पटेल प्रमुख रूप से परदे के पीछे कई महत्वपूर्ण काम कर रहे थे|
उन्होंने कई रिपोर्टों के प्रारूप लिखने में खास मदद की और कई परस्पर विरोधी विचारों के बीच सहमति पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।
राजेन्द्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। सभा में चर्चा रचनात्मक दिशा ले और सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका मिले — यह उनकी ज़िम्मेदारियों में था।
कांग्रेस के इस त्रिगुट के अलावा प्रख्यात विधिवेत्ता और अर्थशास्त्री बी. आर. अम्बेडकर भी सभा के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक थे।
यद्यपि ब्रिटिश शासन के दौरान अम्बेडकर कांग्रेस के राजनीतिक विरोधी रहे थे, परंतु स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर उन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद सँभालने का न्योता दिया गया था।
संविधान की प्रारूप
इस भूमिका में उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया। उनके साथ दो अन्य वकील भी काम कर रहे थे।
एक गुजराती के के. एम. मुंशी थे और दूसरे मद्रास के अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर। दोनों ने ही संविधान के प्रारूप पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए।
इन छह सदस्यों को दो प्रशासनिक अधिकारियों ने महत्वपूर्ण सहायता दी। इनमें से एक बी. एन. राव थे, वह भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे
और उन्होंने अन्य देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का गहन अध्ययन करके कई चर्चा पत्र तैयार किए थे।
दूसरे अधिकारी एस. एन. मुखर्जी थे। इनकी भूमिका मुख्य योजनाकार की थी। मुखर्जी जटिल प्रस्तावों को स्पष्ट वैधिक भाषा में व्यक्त करने की क्षमता रखते थे।
अम्बेडकर के पास सभा में संविधान के प्रारूप को पारित करवाने की ज़िम्मेदारी थी।
इस में कुल मिलकर ३ वर्ष लगे और इस दौरान हुई चर्चाओं के मुद्रित रिकॉर्ड ११ भारी – भरकम खंडों में प्रकाशित हुए।
यह लम्बी मगर दिलचस्प प्रक्रिया थी। संविधान सभा के सदस्यो ने अपने विविध दृष्टिकोण बड़ी सफाई से पेश किए थे।
उसकी प्रस्तुतियों में हम भारत के भविष्य से जुड़े कई मुद्दों पर परस्पर विरोधी विचार देख सकते है
देश के भावी स्वरूप पर, भारतीय भाषाओ, राष्ट्र कौन सी राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्थाएं अपनानी चाहिए, नागरिकों के नैतिक मूल्य कैसे होने चाहिए और कैसे नहीं।
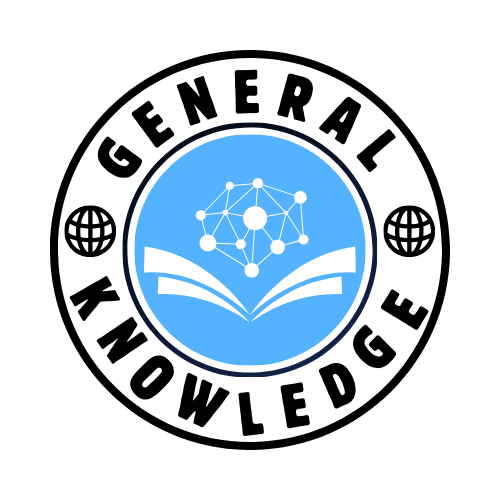

Leave a Reply